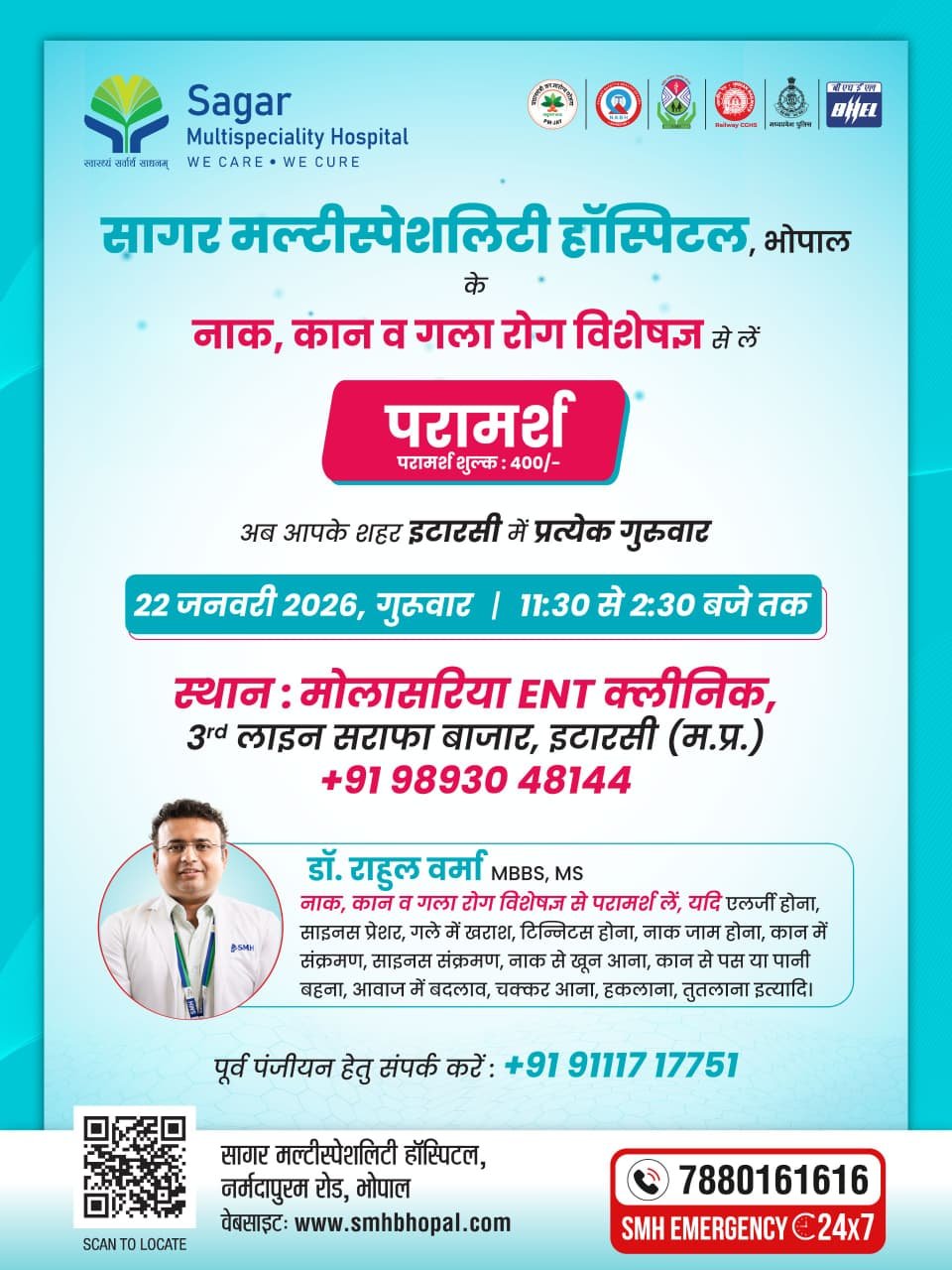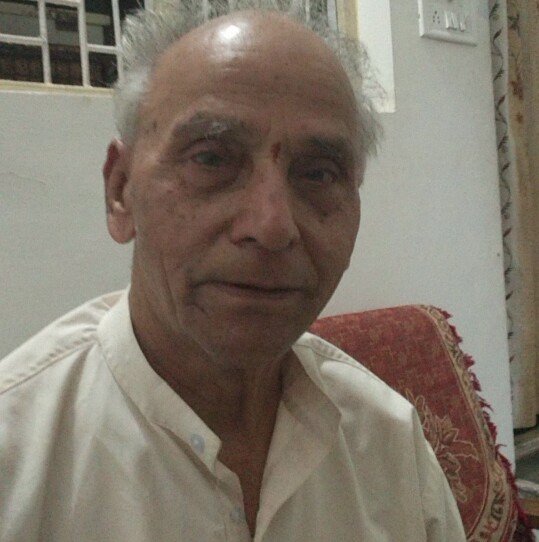- मिलिन्द रोंघे

स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे बड़ी राजनैतिक घटना के रूप में ‘आपातकाल’ को जाना जाता है, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकार विलंबित करने का दुस्साहसपूर्ण कार्य किया था, ‘आपातकाल’ को गांधीवादी विनोबा भावे ने ‘अनुशासन पर्व’ की संज्ञा दी थी। इस मायने में इस घटना का यह स्वर्णजयंती वर्ष भी है। आपातकाल का घटनाक्रम प्रारंभ होता है 1971 से, जब लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से समाजवादी नेता राजनारायण को चुनाव में हराया। श्रीमती गांधी द्वारा चुनावों में प्रशासन का दुरूपयोग करने, भ्रष्ट आचरण, शराब/कम्बल बांटने आदि बिन्दुओं को लेकर राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इस प्रकरण की यह खासियत रही कि इसकी प्रारंभिक सुनवाई देश के अंतिम ब्रिटिश न्यायाधीश विलियम ब्रुस ने की, उनकी सेवानिवृति उपरांत इसकी सुनवाई क्रमश: न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, और न्यायमूर्ति के.एन. श्रीवास्तव के बाद अंतिम सुनवाई न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने की और तमाम प्रकार के दबावों से परे उन्होंने 12 जुलाई 1975 को प्रात: श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करते हुए 6 साल के लिए उन्हेें अयोग्य घोषित कर दिया गया। श्रीमती गांधी के अधिवक्ता धर के अनुरोध पर कि देश में अशांति फैल जावेगी 20 दिन का समय दिया गया। इधर जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए सेना और पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों से अपील की कि सरकार के अवैध आदेश का पालन न करें जैसा की उनका मैन्युअल भी कहता है। इस अपील का सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
श्रीमती गांधी के समर्थन में पार्टी की रैली में ‘इंदिरा इज इंडिया’ का नारा देवकांत बरूआ ने दिया। श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की अपील में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश वी.आर.कृष्ण अय्यर ने 24 जून को यह निर्णय दिया कि श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी व इस क्षमता से संसद में भाषण दे सकेंगी परंतु वेतन लेने व मत देने का अधिकार नहीं होगा। तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण यह संदेश गया कि न्यायपालिका पर विधायिका ने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया। 26 जून 1976 को सुबह राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के अधीन सारे देश में इस आधार पर आपात स्थिति की घोषणा कर दी कि देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
आजादी के बाद यह पहला मौका था, जब देश में आंतरिक स्थिति के नाम पर आपात्काल लगाया गया। इसी दिन समाचार-पत्रों पर भी पाबंदी लगाई गई । जिसके कारण नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार-पत्र 26-27 जून को प्रकाशित नहीं हो सके। 27 जून 1976 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का यह अधिकार छीन लिया, जिसके अनुसार वे विधि के समान संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा और गिरफ्तारी से छूटने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। 29 जून 1976 को एक अन्य अध्यादेश जारी कर आंतरिक सुरक्षा निर्वाह अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया। जिसके अनुसार गिरफ्तारी होने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देने की आवश्यकता नहीं रही।
आपात्काल की घोषणा के बाद देश में विपक्षी नेताओं सहित हजारों लोग रातोंरात बंदी बना लिये गये। उच्चतम न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चार-एक से आपात्काल में सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को स्थगित करने हो सही माना। अन्य चार न्यायमूर्तियों से अहसमति जताने वाले न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने अपने अभूतपूर्व फैसले में लिखा कि ”आदमी के मूलभूत अधिकारों पर कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। यह अधिकार उसे संविधान ने जन्म से दिया है।” इस फैसले पर अमेरिका से प्रकाशित समाचार-पत्र ”वाशिंगटन पोस्ट” ने ”सेल्यूट टू जस्टिस खन्ना” शीर्षक से संपादकीय लिखते हुए उनके निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ के अनुसार ”उस समय देश के नौ उच्च न्यायालयों द्वारा बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया गया था कि आपातकाल हो या न हो लोगों के पास मौलिक अधिकार है और न्याय प्रणाली तक उनकी पहुंच है। दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के फैसले को पलट दिया और ऐसा फैसला दिया जो कानून के शासन में विश्वास करने वाली दुनिया की हर न्यायिक संस्था के इतिहास में काला अध्याय है।” फैसला यह था कि ‘कार्यपालिका की इच्छा पर है कि वह जितना समय तक उचित समझे, आपातकाल लगा सकती है।’
इस फैसले ने देश में ‘तानाशाही, अधिनायकवाद और निरंकुशता को वैधता प्रदान की।’ यदि इसका निष्पक्ष आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि उस समय न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। वस्तुत: यह वह दौर था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मान्य परम्परा को तोड़कर (सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है) अनुच्छेद 124 में दी गई शक्तियों के आधार पर (मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का निरपेक्ष अधिकार है, के तहत) 1973 में अपनी पसंद के न्यायमूर्ति अजित नाथ रे को तीन अन्य जजों (जिन्होंने इस निर्णय के बाद इस्तीफा दे दिया) की वरिष्ठता लांघकर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था और उन्होंने बाद में आपात् स्थिति के फैसलों को वैधानिक बताकर अपनी वफादारी जता दी थी।
इधर लोकसभा में आपात्काल का यह प्रस्ताव 301 के विरूद्ध 76 मतों से एवं राज्यसभा में 147 के विरूद्ध 32 मतों से पारित हो गया। आपातकाल के दौरान ही संसद ने संविधान में 42 वां संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘अखंडता’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को जोड़ा गया था। जितना यह सही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाया (25 जून 1975 को) उतना ही यह भी सही है कि उन्होंने ही स्वयं ही इसे वापस (21 मार्च 1977 को) लेते हुए 18 जनवरी 1977 में आम चुनावों की घोषणा की, लेकिन यह क्यों किया गया। इस विषय पर मतभिन्नता है। कहते हंै कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार सारा देश आपातकाल के समर्थन में आया गया और इससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ गयी। इसके बाद सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया।
जिस विषय पर न्यायपालिका और विधायिका दोषी मानी गई हो, लेकिन विधायिका के रूतबे और डर की वजह से उनकी नीतियों के क्रियान्वयन में कार्यपालिका द्वारा अत्याचार का सहारा लिया गया। नसबंदी कार्यक्रम के टारगेट पूरा करने के चक्कर में अधिकारियों ने जबरदस्ती नसबंदी करानी शुरू कर दी। समाचार पत्रों के अनुसार सिर्फ में 1976 में ही 80 लाख लोगों की नसबंदी की गयी जिसमें अधिकांश पुरूषों की, उनमें से भी अनेक बिना सहमति। सरकार का अधिकारियों पर ऐसा डर था कि अविवाहित युवकों की भी नसबंदी की गयी। हालात ऐसे हो गये कि सरकारी अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों में आने पर नवयुवक एवं पुरूष या तो छिप जाते थे या भाग जाते थे। अधिकारियों की दबिशों के कारण आक्रोश बढऩे लगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनंद मार्ग सहित कुछ संगठनों पर पाबंदी लगा दी गयी। लेकिन आपातकाल के कारण किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, बाद में जनता का यह आक्रोश मतपत्र बाहर आया।
जनसंख्या नियंत्रण का जिस निर्दयता से पालन किया गया उसके कारण परिस्थितियां विपरीत हो गयीं। आपातकाल का यह भी एक पक्ष यह भी सामने आया कि शासकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आई, रेलगाडिय़ां समय पर चलने लगीं और कालाबाजारी पर अंकुश लग गया था। आपातकाल में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिससे श्रीमती गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों मिलते थे, वह थे विनोबा भावे। विगत वर्ष संविधान में 42 वें संविधान संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘अखंडता’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाये जाने के लिए श्री सुब्रम्हणयम स्वामी एवं अन्य द्वारा दायर याचिका की न्यायिक समीक्षा करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसकी कई बार न्यायिक समीक्षा की गयी। संसद ने हस्तक्षेप किया है।
हम यह नहीं कह सकते कि उस समय संसद ने जो कुछ भी किया वह निरर्थक था। बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बने मंत्रिमण्डल ने 44 वॉ संविधान संशोधन कर आपात्काल थोपने की शर्तों को इतना कठिन कर दिया कि शायद ही कोई इसकी पुनरावृत्ति कर सके। 1971 के बाद की राजनैतिक परिस्थितियों में यह भी तथ्य सामने आया, अनेक घटनाक्रम तेजी से घटे जिनमें पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी, अरब-इजराइल युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण महंगाई बढ़ गई, 1973-74 में देश में अकाल की स्थिति निर्मित हो गयी, 1974 में सारे देश में जार्ज फर्नाडिंज के नेतृत्व में रेल हड़ताल (हड़ताल की सफलता को लेकर अनेक बार जार्ज इटारसी आये,) हुई जिसमें हजारों कर्मचारियों पर मीसा लगाकर बर्खास्त (इनमें मेरे पिता भी थे जिन्हें जनता सरकार ने पुन: काम पर लिया), गुजरात और बिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने केन्द्र सरकार को परेशान कर दिया था। जो भी हो ‘आपातकाल’ को कोई भूलना चाहता है और कोई भूलने नहीं देना चाहता।
मिलिन्द रोंघे, द ग्रेंड एवेन्यु कालोनी, इटारसी 9425646588